

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप |
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै: || 41||
ब्राह्मण-पुरोहित वर्गः क्षत्रिय युद्ध और शासन करने वाला वर्ग: विशाम व्यापार और कषि करने वाला वर्ग; शूद्राणाम्-श्रमिक वर्ग; च-और; परन्तप-शत्रुओं का विजेता, अर्जुन; कर्माणि-कर्त्तव्य; प्रविभक्तानि-विभाजित; स्वभाव-प्रभवैः-गुणैः-किसी के स्वभाव और गुणों पर आधारित कर्म।
BG 18.41: हे शत्रुहंता! ब्राह्मणों, श्रत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके स्वरूप के अनुसार तथा प्रकृति के तीन गुणों के अनुरूप विभाजित किया गया है, (न कि इनके जन्म के अनुसार।)
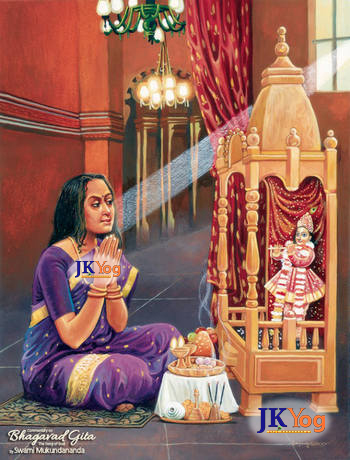
Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!
किसी ने ठीक ही कहा है कि उपयुक्त व्यवसाय की खोज एक उपयुक्त जीवन साथी की खोज करने के समान है। लेकिन हम स्वयं अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय की कैसे खोज करें? यहाँ श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार लोगों का स्वभाव भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है जिससे उनके व्यक्तित्त्व का निर्माण होता है और इसलिए विभिन्न प्रकार के दायित्व उनके लिए सुविधाजनक होते हैं। 'स्वभाव-प्रभवैगुणौ' (मानव स्वभाव और गुण पर आधारित कर्म) के अनुसार वर्णाश्रम धर्म पद्धति समाज की वैज्ञानिक व्यवस्था थी। इस पद्धति के अनुसार समाज में चार आश्रम थे जिन्हें जीवन की चार अवस्थाएँ भी कहा जाता है और चार वर्ण अर्थात् चार व्यावसायिक श्रेणियाँ थी। जीवन की चार अवस्थाएँ इस प्रकार से थीं-(1) ब्रह्मचर्य आश्रम-(विद्यार्थी जीवन) जो जन्म से 25 वर्ष तक की आयु होता था। (2) गृहस्थ आश्रम-यह वैवाहिक जीवन था। यह 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक था। (3) वानप्रस्थ आश्रम- यह 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु तक था। इस अवस्था में मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता था लेकिन वैराग्य का अभ्यास भी करता था। (4) संन्यास आश्रम-यह 75 वर्ष से आगे की अवस्था थी जिसमें मनुष्य अपनी घर गृहस्थी के दायित्वों का त्याग करता था और पवित्र स्थानों में निवास करते हुए मन को भगवान में तल्लीन करता था।
चार वर्णों में ब्राह्मण (पुरोहित वर्ग), अत्रिय वर्ग (योद्धा और शासक वर्ग), वैश्य (व्यापार और कृषि वर्ग वाले), शूद्र (कर्मचारी वर्ग) आते थे। वर्णों में कोई बड़ा या छोटा नहीं माना जाता था। भगवान ही समाज का केन्द्र थे और सभी अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार काम करते थे और भगवत्प्राप्ति के लिए प्रगति करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते थे। इस प्रकार वर्णाश्रम पद्धति में विविधता में एकता थी। विविधता प्रकृति में अंतनिर्हित है और इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। हमारे शरीर में विभिन्न अंग है और ये सब भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सभी अंगों से एक समान कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इन सबको अलग-अलग समझना अज्ञानता नहीं है बल्कि तथ्यात्मक ज्ञान है। समान रूप से मानव जाति के बीच भी विविधता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। समाजवादी देशों में समानता सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है लेकिन वहाँ भी राजनीतिक दलों के नेता हैं जो विचारधारा तैयार करते हैं। वहाँ भी सेना है जो बंदूकों का प्रयोग करती और देश की सुरक्षा करती है। वहाँ किसान भी हैं जो खेती-बाड़ी करते हैं। इन देशों में औद्योगिक श्रमिक भी हैं जो यांत्रिक कार्य करते हैं। समाजवादी देशों में समानता के प्रयासों के बाबजूद भी व्यवसाय के चार वर्ग विद्यमान हैं। वर्णाश्रम पद्धति ने मानवों में विविधता को मान्यता दी और लोगों के स्वभाव के अनुकूल वैज्ञानिक ढंग से उनके कर्त्तव्य और व्यवसाय निर्धारित किए।
यद्यपि समय व्यतीत होने के साथ-साथ वर्णाश्रम पद्धति विकृत हो गयी और वर्गों का निर्धारण स्वभाव की अपेक्षा जन्म के आधार पर होने लगा। ब्राह्मणों के बच्चों ने स्वयं को ब्राह्मण कहना आरम्भ कर दिया भले ही वे अपेक्षित गुणों से संपन्न हों या न हों। उच्च तथा निम्न जाति की अवधारणा भी विकसित हुई और उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों को हेय दृष्टि से देखने लगे। जब यह पद्धति कठोर और जन्म आधारित हो गयी तब यह विरूपित हो गयी। यह एक समाजिक दोष था जो समय के साथ उभरा और यह वर्णाश्रम पद्धति का मूल उद्देश्य नहीं था।
अगले कुछ श्लोकों में इस पद्धति के मूल वर्गीकरण के अनुसार श्रीकृष्ण लोगों के स्वभावों को उनके कर्म के स्वाभाविक गुणों के साथ चित्रित करेंगे।